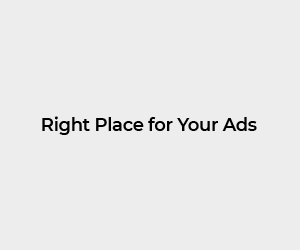Munshi Premchand – बनारस के प्रेमचंदेश्वर महादेव, मुक्तिबोध के भगवान
बनारस में प्रेमचंद के अनेक संस्मरण हैं. कहीं वे नेहरू से बौद्धिक विमर्श कर रहे हैं, तो कहीं उन्हें महादेव का स्वरूप मान कर पूजा जा रहा है. उनकी जयंती पर पढ़ें इन रंगों और दृश्यों से रचा गया काशी के प्रतिनिधि स्वर व्योमेश शुक्ल का यह लेख.
मुक्तिबोध ने लिखा था : ‘मेरी मां ने मुझे प्रेमचंद का भक्त बनाया’.
मुझ न कुछ को लिखना होगा कि मेरी मां और यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा ने मुझे प्रेमचंद का भक्त बनाया.
हुआ यह कि क्रिकेट, स्थानीय निकाय के चुनाव, इश्क़, केबल टीवी और हस्तमैथुनादि की चकल्लस में दो साल तक कुछ न पढ़ने के बावजूद इंटरमीडिएट की परीक्षा तो देनी ही थी. मुझे जबरन पढ़ने के लिए बिठाया जाने लगा. गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान में तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं था, सो मैं हंस प्रकाशन वाली प्रेमचंद की कहानियों की छोटी सी रंग-बिरंगी किताब के साथ बैठा रहता.
वर्ष 1996 की वसंत ऋतु में वह रात का अनोखा शुभ समय था, जब मैं पहली बार किसी लिखी हुई चीज़ के प्यार में गिरफ़्तार हुआ. कहानी का नाम था ‘सुजान भगत’.
प्रेमचंदेश्वर महादेव
अब लमही को गांव मानना मुश्किल है. कुछ समय पहले, वाराणसी विकास प्राधिकरण में बाक़ायदा शामिल होने के बाद से वह बनारस का एक बिगड़ा हुआ मुहल्ला ही है जहां मुख्य रूप से तीन जातियाँ रहती हैं—गोड़, कुनबी और कायस्थ. प्रायः सभी कायस्थ खुद को प्रेमचंद का दूर या नज़दीक का रिश्तेदार बताते हैं. समृद्धि में कुनबी समुदाय के लोगों ने सबको पीछे छोड़ दिया है. वे दरअसल प्रदेश की सबसे ताक़तवर पिछड़ी जातियों में से एक हैं.
उपन्यास-सम्राट के मक़ान के ठीक बाहर एक शिव मंदिर है. उसके निर्माण की दास्तान तथाकथित रूप से 150 साल और वास्तव में 10-15 साल पुरानी है.
हालांकि इस बीच वहां जाने पर मंदिर के ऊपर ‘प्रेमचंदेश्वर महादेव’ लिखा हुआ नहीं मिला. उसकी बजाय वहां लिख दिया गया है : ‘बाबा भोलेनाथ मंदिर, लमही’. साथ ही, दर्जन भर शिवलिंग और स्थापित हो गये हैं.
बनारस का सदा सनातन साधारण मन महत व्यक्तित्वों और प्रवृत्तियों को ऐसे ही स्वीकार करता है. महाप्राण निराला के जीवन और कृतित्व के मर्मज्ञ विद्वान प्रोफ़ेसर बच्चन सिंह ने बनारस के एक मुहल्ले रथयात्रा-स्थित नई कॉलोनी में अपना घर बनाया. नगर महापालिका ने उन्हीं की सलाह पर निराला को प्रणति अर्पित करते हुए कॉलोनी का नाम रखा निराला निवेश. कालांतर में, उसी कॉलोनी में महादेव के एक सर्वथा अभिनव अवतार विकास प्राधिकरण के छोटे से उद्यान में प्रतिष्ठित हो गए—उनका नाम पड़ा ‘निरालेश्वर महादेव’.
विज्ञ बनारस-प्रेमी जानते हैं कि बनारस में महादेव के ऐसे ही अनेक चित्र-विचित्र स्वरूप जीवंत और मूर्तिमान हैं—क़र्ज़ के बोझ से छुटकारा दिलानेवाले ‘ऋणमुक्तेश्वर महादेव’ और बुख़ार भगानेवाले ‘ज्वरहरेश्वर महादेव’.
घर में औचक किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर स्त्रियां जिन मातृशक्ति को साक्षी मानकर अपने आंचल में उस वस्तु विशेष के फिर से मिल जाने की कामना के साथ एक नन्हीं सी गांठ बांध लेती थीं उन देवी का नाम था ‘अचक्का माई’. उनका मंदिर अब भी जागता है. आज भी जब कुछ खोया हुआ वापस मिल जाता है, लोग उन देवी के दरबार का दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं. काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में भी ऐसे ही एक ग्राम देवता प्रतिष्ठित हैं : ऐसा कहा जाता है कि जिन युवकों के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें उक्त देवता का नियमित दर्शन करना चाहिए. ग्रामदेवता का नाम भी बड़ा प्रासंगिक है : ‘अकेलवा बाबा’.
यह तालाब आप सबकी है
प्रेमचंद के आख़िरी दिन बनारस के जिस मकान में बीते और जहाँ उनकी मृत्यु हुई, उस विराट परिसर के ठीक सामने ‘रामकटोरा’ नाम का पोखरा है. उसी की वजह से मुहल्ले का नाम भी रामकटोरा है. मैं इस पोखरे से कुछ ही दूर रहता हूं. प्रेमचंदजी जब मुंबई से निराश होकर लौटे थे, तब जयशंकर प्रसादजी की सिफ़ारिश पर भारतेन्दु हरिश्चंद्र के परिवार ने उन्हें यह सौम्य रिहाइश दी थी.
यहां प्रेमचंद के सपरिवार रहने की बात सबसे पहले मां ने मुझे बताई थी. तब मैं किशोर था और हंस प्रकाशन की छोटी-छोटी सुंदर पुस्तिकाओं में प्रकाशित उनकी अनेक कहानियां पढ़ चुका था. बाद में अमृत राय की लिखी प्रेमचंद की जीवनी ‘कलम का सिपाही’ पढ़ते हुए इस बात का सत्यापन भी हो गया. कुछ और समय बाद, जब लेखक बनने का शौक़ हुआ तो मैंने ऐसी कल्पनाएं भी कीं कि प्रेमचंद कभी-कभी इस पोखरे की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ लिखते-पढ़ते होंगे. ज़ाहिर है, वे उनके आख़िरी बरस थे, तो ज़रूर ‘साहित्य का उद्देश्य’, ‘क़फ़न’ या ‘गोदान’ की कुछ बातें उन्होंने इसके प्रशस्त किनारों पर टहलते हुए सोची होंगी. मेरी कल्पना में दम था. उसकी बुनियाद में यथार्थ की शक्ति थी.
नब्बे के दशक के शुरुआती कुछ सालों तक उस पोखरे के परिसर में एक व्यायामशाला भी थी जहां कुछ दिशाहारा नौजवान कसरत किया करते थे. प्रेमचंदजी के घर वाले हिस्से पर तो ख़ैर आज़ादी के बाद से ही पंखे और वाटर पंप बनाने वाली कंपनी का कारख़ाना खुल चुका था, जिसमें अंदाज़न पांच हज़ार लोग काम करते रहे होंगे. लेकिन तभी, न जाने क्या हुआ कि मुहल्ले के शरीफ़ परिवारों को अखाड़े और उसमें आने-जाने वाले कुछ लोगों से दिक़्क़त होने लगी. उन्होने एक अभियान चलाकर और चिट्ठी-पतरी, पुलिस-कचहरी करके अखाड़ा बंद करा दिया.
बहरहाल, जो होना था, हुआ. सड़क के उस पर कारख़ाना बंद हुआ और इस पार अखाड़े का पटाक्षेप हो गया. पोखरे के परिसर में देवताओं के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा हुई, नियमित अनुष्ठान शुरू हुए, विवाहिता स्त्रियां अपनी सासों, ननदों और बाल-बच्चों के साथ वहां आने लगीं और एक साधु अपने कुछेक शिष्यों के साथ उसी परिसर में रहकर प्रवचन करने के लिये बसा दिये गये. नियमित प्रवचन का सिलसिला चरित्रहीनता और चढ़ावे में घपले के आरोप में साधु और उनकी मंडली के निकाल बाहर किए जाने तक चलता रहा.
इस बीच जिन कुछ लोगों के घर पोखरे के किनारे थे, मेरा ऐसा शक़ है, कि उन्होंने अपनी सीवेज पाइपों को भीतर ही भीतर सरलता से पोखरे में मिला दिया. पोखरे के जल से दुर्गंध उठने लगी और जलकुंभी के उग आने की वजह से पानी दिखना भी बंद हो गया. सीढ़ियों पर काई जमा हो गई. सीढ़ियों पर चलना ख़तरे से ख़ाली नहीं रहा तो कुंड को ईंट और सीमेंट की दीवार से घेरकर उसके दरवाज़े पर ताला लगा दिया गया और दरवाज़े के शिलापट्ट पर पोखरे का नामकरण भी कर दिया गया—‘प्राचीन एवं धार्मिक रामकटोरा कुंड’. इस प्रकार पोखरा कुंड हो गया. कुंड सड़क किनारे पड़ता था तो राह चलते लोग उसे डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करने लगे.
कुछ बरस पहले तक एक सूचनापट्ट भी वहां लगा हुआ था, जिस पर और कुछ हिदायती वाक्यों के साथ मुझ-जैसों को यह लिखकर याद दिलाया गया था कि ‘यह तालाब आप सबकी है.’
लेकिन समय यत्किंचित बदला है. कुंड साफ़ हो गया है. उसमें बाहर से कूड़ा फिंकना भी बंद हुआ है; लेकिन राह चलते कूड़ा तालाब में न फेंका जा सके, इसलिए उसे सड़क की ओर लोहे की जाली और कारख़ाने की समाधि पर बने अंगरेज़ी माध्यम स्कूल के विज्ञापनों की बड़ी चादरों से ढंक दिया गया है. मंदिर भी ज़्यादा सार्वजनिक हुआ है. भक्तगण—स्त्री, पुरुष और बच्चे— वहां आते हैं, दर्शन-पूजन करते हैं और कभी-कभी फ़ुर्सत से तालाब की मछलियों को चारा भी खिलाते हैं. बस इस पूरे दृश्यालेख में प्रेमचंद कहीं नहीं हैं.
शहर बनारस के गोदौलिया और धूपचंडी जैसे मुहल्ले या बेनियाबाग़ पार्क—जहां के भूगोल में प्रेमचंद सांस लेते, टहलते और रह-रहकर अपने ख़ास अंदाज़ में अट्टहासपूर्वक हंसते थे—जैसी जगहों पर प्रेमचंद की उपस्थिति का कोई स्मारक नहीं बन सका. वहां पहुंचकर उपन्यास-सम्राट का कोई सुराग़ नहीं मिलता. हां; लहुराबीर और पांडेपुर चौराहे पर उनकी प्रतिमाएँ अवश्य लगी हुई हैं. पांडेपुर से प्रेमचंदजी के जन्मस्थल लमही की दूरी 4 किलोमीटर है. इसी रास्ते पर विकास प्राधिकरण ने सड़क के बीचोंबीच लगे बिजली के खंबों पर रात के अँधेरे में एलईडी बल्बों से जगमगाने वाली पुस्तिकाएं लगाई हैं. उन पुस्तिकाओं में किसी के भीतर लिखा है ‘गोदान’; किसी पर ‘रानी सारंधा’ और किसी पर ‘बड़े घर की बेटी’.
मुंशी नहीं; प्रेमचंद
एक ज़माने में के. एम. मुंशी और प्रेमचंद संयुक्त रूप से ‘हंस’ के संपादक थे. उस पत्र में संपादकों का नाम क्रमशः बायीं और दाहिनी ओर यों लिखा रहता था— संपादक : ‘मुंशी प्रेमचंद’; जिसमें मुंशी का मतलब था के. एम. मुंशी और प्रेमचंद. 57 वर्षों के छोटे से जीवन में प्रेमचंद पेशे से मुंशी थे भी नहीं; पहले अध्यापक और बाद में पत्रकार-संपादक थे.
दरअसल मुंशी अरबी भाषा का पुल्लिंग शब्द है, जिसके विभिन्न अर्थ इस प्रकार हैं—गद्य लेखक, अदीब, लिपिक, क्लर्क, वकील का मुहर्रिर, कचहरी में अर्ज़ियां लिखनेवाला, जिसकी लिखावट अच्छी हो, आरंभ करने वाला, लिखने वाला, सचिव, किसी कार्यालय में लिखने का काम करनेवाला लिपिक, लेख या निबंध आदि लिखनेवाला लेखक; पंडित; विद्वान; बही-ख़ाता लिखने वाला व्यक्ति, वक़ील का सहायक; पेशकार; कायस्थ समाज में प्रयुक्त एक संबोधन तथा कुलनाम या सरनेम.
तो क्या अपने-अपने आशय से लोगों ने प्रेमचंद के नाम के आगे मुंशी लगाना शुरू कर दिया? शायद हां. शायद नहीं, क्योंकि उनकी उनकी जीवन-संगिनी शिवरानी देवी और बेटे अमृत राय ने भी अपनी-अपनी पुस्तकों में प्रेमचंदजी के लिए अनेकशः इस शब्द का प्रयोग किया है. एक सदी पहले उत्तर भारत के कायस्थों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था. और अब? यह हाल है कि अगर आप प्रेमचंद के नाम के आगे मुंशी न लगाएं तो माना जायेगा कि किसी और प्रेमचंद की बात हो रही है. तब मुंशी क्यों? ज़ाहिर है कि उत्तर भारत में कायस्थ जाति के लोगों को बोलचाल में मुंशीजी कह दिया जाता है. तो क्या यह उनके कायस्थ जाति का होने की ओर एक इशारा है? एक छिपा हुआ जातिसूचक संबोधन? ताकि मृत्यु के नवासी साल बाद भी उनकी जाति लोगों को याद रहे? नहीं. आज जो महज़ जातिसूचक है, कभी वह सम्मानसूचक था.

हिंदी को लेकर नेहरू की फ़िक्र और निराला का प्रत्युत्तर
बनारस की एक गोष्ठी में खींची गई इस क्लैसिक तस्वीर को देखकर मन उदास हो जाता है, जबकि युग विशेष के अनेक मूर्धन्य इस तस्वीर में हैं. फ़ोटो देखते ही हिंदी के अमर कवि निराला की याद आ जाती है, जो इस समूहन में नहीं हैं. अपने गद्य-संग्रह ‘प्रबंध-प्रतिमा’ में प्रकाशित संस्मरणात्मक निबंध ‘नेहरू जी से दो बातें’ में निराला ने रेलगाड़ी के डिब्बे में हुई उस मुलाक़ात को याद किया है, जिसमें वह क्षुब्ध होकर नेहरूजी से मिले थे और बनारस की इस गोष्ठी का ज़िक्र उनसे किया था.
असल में जवाहरलाल नेहरू के सन 1935 में काशी आगमन पर बांसफाटक मुहल्ले में पंडित रामानंद मिश्र के आवास पर ‘रत्नाकर रसिक मंडल’ की ओर से उनका अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ था. बीच में जवाहरलाल जी और उनके पीछे श्रीमती कमला नेहरू को पहचाना जा सकता है. बाएं से क्रमशः दिनेशदत्त झा, जयशंकर प्रसाद, सांवलजी नागर, लक्ष्मीकांत झा और जनार्दन झा ‘द्विज’ हैं. एक व्यक्ति को नहीं पहचाना जा सका. पीछे की पंक्ति में कांतानाथ पांडेय ‘चोंच’, कविराज प्रताप सिंह और गणेशदास जी हैं और दाहिनी ओर क्रमशः शिवप्रसाद मिश्र ‘रूद्र’, बाबू संपूर्णानंद, बलदेवप्रसाद मिश्र, रामानंद मिश्र, ज्योतिभूषण गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, एक अज्ञात सज्जन और भवेशदत्त झा हैं.
इसी गोष्ठी में नेहरूजी ने कहा था कि ‘हिंदी में दरबारी ढंग की कविता प्रचलित है.’ महाप्राण निराला ने अख़बारों में यह बात पढ़ी और बहुत बुरा माना. जब नेहरूजी लौट रहे थे तभी लखनऊ रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के डिब्बे में निराला उनसे मिले और कहा:
बनारस के जिन साहित्यिकों की मंडली में आपने दरबारी कवियों का उल्लेख किया था, उनमें से तीन को मैं जानता हूं. तीनों अपने-अपने विषय के हिंदी के प्रवर्तक हैं. प्रसादजी काव्य और नाटक साहित्य के, प्रेमचंदजी कथा-साहित्य के और रामचंद्रजी शुक्ल आलोचना-साहित्य के. आप ही समझिए कि इनके बीच आपका दरबारी कवियों का उल्लेख कितना हास्यास्पद हो सकता है. इन्होंने सम्मान के लिए आपको बुलाया था, इसलिए आपके विरोध में कुछ नहीं कहा. खड़ी बोली की प्रतिष्ठा के बाद जो काव्य मैदान में पैर रखता और आगे बढ़ता है, उसके साथ दरबारीपन का कोई संबंध नहीं.
बनारस के जिन साहित्यिकों की मंडली में आपने दरबारी कवियों का उल्लेख किया था, उनमें से तीन को मैं जानता हूं. तीनों अपने-अपने विषय के हिंदी के प्रवर्तक हैं. प्रसादजी काव्य और नाटक साहित्य के, प्रेमचंदजी कथा-साहित्य के और रामचंद्रजी शुक्ल आलोचना-साहित्य के. आप ही समझिए कि इनके बीच आपका दरबारी कवियों का उल्लेख कितना हास्यास्पद हो सकता है. इन्होंने सम्मान के लिए आपको बुलाया था, इसलिए आपके विरोध में कुछ नहीं कहा. खड़ी बोली की प्रतिष्ठा के बाद जो काव्य मैदान में पैर रखता और आगे बढ़ता है, उसके साथ दरबारीपन का कोई संबंध नहीं.
नेहरू सहसा हिंदी साहित्य की प्रगति को लेकर चिंतित और हताश हो उठते थे और अपनी राय से जाने-अनजाने प्रेमचंद, आचार्य शुक्ल, प्रसाद और निराला जैसे हिंदी के कालजयी लेखकों को क्षुब्ध और दुखी कर देते थे. इसके बाद नेहरू ने ‘विशाल भारत’ के किसी अंक में किसी की लिखी यह बात पढ़ ली थी कि हिंदी-साहित्य ने बहुत उन्नति कर ली है और उसमें शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ उत्पन्न हो गए हैं. उन्होंने मित्रों से कुछ पुस्तकें मंगवाकर पढ़ भी डालीं और हताश हो गए और हताशा के फलस्वरूप नवंबर 1935 के ‘विशाल भारत’ में उन्होंने साहित्य-संबंधी एक नोट लिखा.
निराला तो क्रोधी थे. उन्होंने अपना गुस्सा नेहरूजी से कहासुनी करके ठंडा कर लिया था; लेकिन प्रेमचंद ने बारीक़ राह ली : ‘हंस’ के जनवरी 1936 अंक के संपादकीय में उन्होंने लिखा:
जब पढ़े-लिखे लोग हिंदी लिखना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, जब हमारे नेता हिंदी-साहित्य से प्रायः बेख़बर-से हैं, जब हम लोग थोड़ी-सी अंगरेज़ी लिखने की सामर्थ्य होते ही हिंदी को तुच्छ और ग्रामीणों की भाषा समझने लगते हैं, तब यह कैसे आशा की जा सकती है कि हिंदी में ऊंचे दर्जे के साहित्य का निर्माण हो…..जिस चीज़ का कोई पुछंतर नहीं, वह अगर नेहरूजी को निराश करती है तो कोई आश्चर्य नहीं.
इसी लेख में आगे चलकर एक बहुत करारा आत्मव्यंग्य भी है:
हमारे यहां वही साहित्य की सेवा करते हैं, जिन्हें कोई काम नहीं मिलता, या जो लोग केवल मनोविनोद के लिए कभी-कभी कुछ लिख-पढ़ लिया करते हैं. ऐसे अरसिक समाज में उच्चकोटि का साहित्य क़यामत तक न आएगा.
क्या इस उद्धरण में हिंदी के बारे में नेहरूजी के विचारों की संस्तुति या अनुमोदन है? प्रेमचंद का मनुष्य और साहित्य, राजनीति के किसी भी संस्करण से आलोचनात्मक दूरी बरतते हुए बना-बढ़ा है. मौक़ा आने पर एक कर्त्तव्यनिष्ठ पत्रकार की तरह वह राजनीति पर टिप्पणी करते हैं; लेकिन उसका कमतर अनुषंग बन जाने की बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकते. उनका साहित्य, उन्हीं के शब्दों में, ‘राजनीति के आगे चलने वाली मशाल’ है. Credit The wire